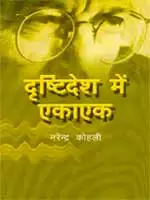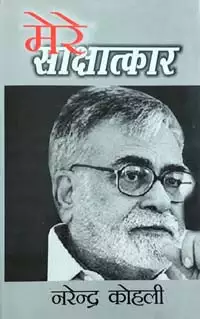|
कहानी संग्रह >> दृष्टिदेश में एकाएक दृष्टिदेश में एकाएकनरेन्द्र कोहली
|
6 पाठक हैं |
|||||||
ये कहानियाँ भी आज मेरे लिए अपने लेखकीय-जीवन के पुराने एलबम को उलटने के ही समान हैं
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
ये कहानियाँ भी आज मेरे लिए अपने लेखकीय-जीवन के पुराने एलबम को उलटने के
ही समान हैं; किंतु इनमें पिछले संकलन के कुछ बाद के जीवन के चित्र हैं।
ये उस काल की कहानियाँ हैं जब मेरा लेखक अपने दुःख-दर्द के साथ-साथ दूसरों
के दुःख-दर्द भी पहचानने लगा था। इनमें से अधिकांश कहानियाँ अपने जीवन को
छूते हुए अन्य लोगों के अनुभव के क्षेत्रों की कहानियां हैं। कदाचित् मेरी
लेखकीय सहानुभूति इन्हीं दिनों विकसित होनी आरंभ हुई थी। जीवन के केन्द्र
में अब भी कॉलेज ही था, किंतु छात्र से अध्यापक बनने की प्रक्रिया से गुजर
चुका था। नई नौकरी, विवाह, दाम्पत्य जीवन की कुछ समस्याएं, और इनके कारण
दूसरों के जीवन में उत्पन्न होती हुई जटिलताएं-जीवन के इन नए अनुभवों ने
अपनी आकस्मिकता के कारण वाणी की वक्रता को गौण बना दिया था, अनुभूतियां ही
प्रधान हो गई थीं।
मिल का मॉडल
नए मरीज़ की अवस्था बहुत ही ख़राब थी। किसी भी समय उसकी हालत बिगड़ सकती
थी। और अस्पताल में भी यदि हालत बिगड़ जाए तो अर्थ एक ही
है—मृत्यु !
सायरा कह रही थी कि जब वह लाया गया था तो और भी बुरी अवस्था में था। पायलट अफसर था कोई। जहाज़ से गिर पड़ा था और उसे खेतों में पड़े हुए को उठा लाए थे। और मैं सोच रही थी—सिविलियन जहाज़ों में तो यही बुरी बात है कि एक ही आदमी को जहाज़ देकर उड़ा देते हैं। उसे कुछ हो जाए तो बचानेवाला भी न हो। सैनिक जहाज़ों में शायद ऐसा न होता हो—मुझे पता भी क्या है। मैं कौन सी एयरफोर्स में काम कर चुकी हूं।
और अब, जब नाइट ड्यूटी पर आई तो मैंने उस नए मरीज़ को देखा। साथ ही, परिचय भी मिला। पट्टियों में बंधा पड़ा था वह। स्वभावतः मुझे उत्सुकता हुई। मैंने ध्यान से देखा उसे। कोई नई बात नहीं थी। रोज़ ही मरीज़ देखती हूं। नर्स हूं—पेशा ही यही है। बच्चा पैदा करने से पूर्व मां को तड़पते देखा है। पैदा होते हुए और धरती पर आने पर हाथ-पैर पटकते हुए बच्चे को देखा है। मां की वह गर्व भरी मुसकान भी देखी है। और उन्हें छोटे-बड़े बच्चों को निरीह, बिस्तर पर पड़े तड़पते भी देखा है। कितना बेचारा-सा लगता है व्यक्ति—अस्पताल के इन बिस्तरों पर पड़ा हुआ, जैसे बच्चा हो छोटा-सा। करवट बदल दूं तो बदल लेगा, नहीं तो एक ही करवट पड़े सोता-जागता रहेगा। और मृत्यु से लड़ता हुआ आदमी ! ओफ ! कैसे हाथ-पैर मारता है। अंत में शांत होकर पड़ा रहता है। रोज़ ही देखती हूं। सत्य तो यह है कि मरे-जीते आदमी में विशेष अंतर नहीं लगता मुझे। दो अवस्थाएं मात्र हैं आदमी की ये !
पर यह मरीज़-नया मरीज़—उन लोगों में से नहीं लगता मुझे। यह नहीं मरेगा—यह मैं जानती हूं। अपने इंस्टिक्ट से ही बता सकती हूं कि यह नहीं मरेगा, क्योंकि यह जीना चाहता है। उसके बेहोश मुख की लकीरों में ऐसी कोई बात नहीं थी, जो उसे मृत्यु से आशंकित बताती। वह जिएगा।
वैसे इस समय तो उसकी हालत खराब ही थी। पट्टियों से यूं बंधा पड़ा था कि उसकी अपनी मां भी शायद उसे इस हालत में पहचान न सके।
सोचती हूं, उसकी मां अपने घर में बैठी होगी संतोष से। क्या कर रही होगी ? शायद अपने इसी बेटे के लिए जुराबें बुन रही हो—सर्दियां आ रही हैं न ! सोचती होगी कि बेटा अपनी फ्लाइट से वापस आएगा तो उसे जुराबें देगी। और बेटा यहां पड़ा है—बेहोश ! डॉक्टर अभी तक यह आश्वासन भी नहीं दे सके कि वह जी ही पड़ेगा। पर मैं कहती हूं, वह जिएगा। नर्स किसी डॉक्टर से कम तो नहीं होती है।
पर कौन जाने उसकी मां भी किसी अनदेखे भय, किसी आशंका के कारण बिस्तर पर करवटें बदल रही हो। अपने बेटे की खैर मना रही हो। कहते हैं कि खून के रिश्ते में इस प्रकार की घटनाओं का आभास हो जाया करता है। और इसकी मां तो जानती ही होगी कि उसका बेटा हवा में उड़ रहा है—जहां किसी क्षण भी दुर्घटना हो सकती है।
पर मैं मां के विषय में ही क्यों सोच रही हूं ? मैं उसकी पत्नी के विषय में क्यों नहीं सोचती ? वह क्या कर रही होगी ? यदि विवाहित न भी हो उसकी प्रेमिका तो होगी ही। पायलट है—कोई एयर-होस्टेस या कोई और। प्रेमिका तो होगी ही—पर प्रेमिका ! पत्नी ही हो तो ठीक है।
सायरा ठीक कहती है कि मेरे इंग्लैंड जाने का कोई लाभ नहीं हुआ। छह वर्ष रहकर आई हूं इंग्लैंड में, पर अब भी दक़ियानूसी हिन्दू लड़कियों के समान मां या पत्नी की ही बात अधिक सोचती हूं, प्रेमिका की कम। मुझसे तो वे एंग्लो-इंडियन लड़कियां ही अधिक एडवांस्ड हैं, जो कभी भारत की सीमाओं को पार कर कहीं नहीं गईं—किन्तु प्रत्येक बात इंग्लैंड की दृष्टि से ही सोचती हैं।
पर सायरा एक बात नहीं जानती। मैं मां और पत्नी के रूप में अब भी नहीं सोचती—अब ही सोचती हूं। जब मैं इंग्लैंड में थी और मेरा बाबी मेरे पास था, तब तो कभी मैंने दक़ियानूसी हिन्दू लड़कियों के समान नहीं सोचा था। तब मैं अपने परिवार के बारे में, अपने भाई-बहनों के बारे में कभी नहीं सोचा था। तब मैंने बाबी के घरवालों के विषय में भी नहीं सोचा था। तब मैं थी और मेरा बाबी था। हम व्यक्ति थे, परिवारों से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं था। मैं तब प्रेमिका मात्र थी...न पत्नी थी, न कुलवधू, और इसलिए मां भी नहीं थी।
पर उन दिनों मैं जवान थी। आठ वर्ष बीत चुके हैं उस बात को। कुल बीस वर्षों की हुआ करती थी मैं। तब की बातें अब नहीं हैं। उसके पश्चात् कितना जीवन देखा है मैंने। कितना घूमी हूं। यह आठ वर्षों का, खानाबदोश का-सा जीवन। कुछ महीने कहीं, कुछ महीने कहीं। कोई घर नहीं, परिवार नहीं। जीवन से पृथक, कटे-छंटे से होटल ! वह भी कोई जीवन है—आडम्बर !
अब मैं थक गई हूं। उन दिनों के समान हर समय टिप-टाप, सजी-धजी नहीं रह सकती। हमेशा अकड़कर बैठ नहीं सकती। अट्ठाईस वर्षों का होकर, अब जीवन स्वयं को ढीलना चाहता है। रेस्तराओं, होटलों और पार्टियों के जीवन से तंग आ गई हूं। अब तो एक छोटे से घर की इच्छा होती है, जिसमें दो-एक कमरे हों—जो मेरे अपने हों, जिनकी सफाई मैं स्वयं करूं। रसोई हो, मेरी अपनी। बहुत सारे डिब्बे हों साफ़-सुथरे ! उन पर लिख-लिखकर मैं अपने हाथों से लेबिल लगाऊं। उनमें से चीज़ें निकाल-निकालकर पकाऊं और अपने पति और छोटे-छोटे दो-एक बच्चों को खिलाऊं। जब डिब्बे खाली हो जाएं तो एक-एक डिब्बा देखकर पति को लिखाऊं—दाल चने की दो सेर, दाल मसूर की डेढ़ सेर—अब स्वयं साथ जाकर सामान लाने की इच्छा नहीं होती। वे जाएं और ले आएं। रसोई तक ही सीमित हो जाऊं। इन्हीं दीवारों में घुट जाऊं।
और उस घर में एक गुसलखाना भी हो। जब वे काम पर चले जाएं तो मैं अपने गंदे बिखरे बालों का—जिनमें झाड़ू करते हुए या चूल्हा फूंकते हुए धूल और राख पड़ गई हो—रद्दी-सा जूड़ा बनाऊं और छोटे-बड़े अनेक कपड़े लेकर धोने बैठ जाऊं। उसमें उनकी बनियानें हों, कच्छे हों, रुमालें हों, पाजामें हों, कुर्ते हों। पैंट-कमीज़ तो धोबी से ही धुलवाऊंगी। चादरें हों, छोटी-छोटी कमीज़ें हों और एक छोटी-सी फ़्राक ! अंत में एक साड़ी या सलवार कमीज़ मेरी भी हो।
गार्डन हो, जिसमें....
‘‘सिस्टर ! सिस्टर !’’ वह कोने के बेडवाला मरीज़ हमेशा ही रात को पुकारता है। नींद नहीं आती बेचारे को। वह कहता है कि मैं उसे नींदवाली गोलियां दूं---किन्तु क्या लाभ है उन गोलियों का ! सिस्टम बिगड़ जाता है।
‘‘क्या बात है, बेड नम्बर तेरह ?’’ मैं मुसकराई।
मैं हमेशा बेड नम्बर से ही पुकारती हूं मरीज़ों को। अच्छा लगता है मुझको। वे भी मुसकराते हैं कि वे आदमी न होकर बेड नम्बर हो गए हैं।
‘‘नींद नहीं आती, सिस्टर !’’ बेड नम्बर तेरह मुसकराया।
आगे वह कुछ बोला नहीं, पर मैं जानती थी कि वह नींद की गोलियां मांग रहा है।
मुझे दया-सी आ गई। देखो, बेचारे को नींद के लिए भी रोज़ गोलियां मांगनी पड़ती हैं। ‘‘सो जाओ, बेड नम्बर तेरह !’’ मैंने उसके माथे पर हाथ रखा, ‘‘सोने की कोशिश करो, नींद आएगी।’’
मैंने उसका कंधा थपथपाया और लौट आई। मैं जानती थी, वह सो जाएगा।
मुझे लगता था, ये सब मेरे बच्चे हैं। मैं मां हूं इनकी। इनकी नींद सोती हूं और इन्हीं की नींद जागती हूं। ये बच्चे हैं, जिद्दी बच्चे ! सोने से पहले चाकलेट मांगते हैं, टाफियां मांगते हैं और मेरे मनाने पर मानकर सो जाते हैं।
मेरा अपना घर होगा, तो मैं अपने बच्चों को भी सुलाया करूंगी। कोई ज़िद करेगा तो उसे एक-आध चांटा लगा दूंगी। वह रो पड़ेगा तो मैं भी उसके साथ रो पड़ूंगी, ‘हाय, मेरे लाल !’
क्या हो गया है मुझे। मुझे अपने बच्चों के बदले इन मरीज़ों का ख़याल करना चाहिए। नया मरीज़ कितने मज़े से सो रहा है—हैल्दी स्लीप ! उसे कोई खतरा नहीं है। वह जिएगा, क्योंकि वह शायद किसी के लिए जीना चाहता है। मैं भी किसी के लिए जीना चाहती हूं। कितने समीप हैं हम !
दूसरे दिन जब मैं आई तो मेरा ध्यान सबसे पहले नए मरीज़ की ओर गया। वह खतरे की सीमाओं को बहुत पीछे छोड़ आया था। मैं सोचती हूं कि यदि सिविलियन के स्थान पर वह सैनिक पायलट होता तो ज़्यादा अच्छा होता। वह मृत्यु से किस प्रकार जूझा था, यह मैंने देखा था। एक क्षण के लिए भी वह निराश नहीं हुआ था। ठीक कहा था डॉक्टर पुरी ने, ‘ही हैज़ विल !’ और अब तो कोई बात ही नहीं थी। घाव अब भी उतने ही गहरे थे। पीड़ा अब भी उसे उतनी ही हो रही होगी, किन्तु जान का खतरा अब नहीं रह गया था उसे।
धीरे-धीरे नया मरीज़ भी पुराना हो गया था। उसके परिवार वालों का पता लग गया था। वे आते थे उससे मिलने। मां थी उसकी—बूढ़ी-सी। एक बहन थी छोटी। सुन्दर नहीं कही जा सकती, किन्तु आकर्षक अवश्य थी। गोरी झक्क ! अच्छी फैशनेबुल लड़की थी। और उसके दो भाई आए थे मिलने।
अश्विनी...नया मरीज...अधिक बातें नहीं करता था। बस मुसकराता जाता था। मैंने उसे अपनी मां से भी अधिक बातें करते नहीं देखा था। भाइयों के दुर्घटना के विषय में पूछने पर बस यही कहा था उसने, ‘मशीनरी गड़बड़ा गई और गिर गए।’ और अंत में एक मुसकान जोड़ दी थी उसने।
बहन बहुत सारी बातें करती रही थी। वह सुनता रहा था। मुझे लगा, उसकी यह छोटी बहन ही सबसे अधिक समीप है उसके। वे शायद भाई-बहन के औपचारिक रिश्ते से ऊपर उठकर मैत्री स्तर पर आ चुके थे। अच्छा लगा मुझे। इंग्लैंड जाने से पहले, मेरी भी भैया से ऐसी ही दोस्ती थी। पर फिर मैं इंग्लैंड चली गई थी। मुझे बाबी मिल गया था। मुझे और किसी की ज़रूरत भी नहीं रही थी और वैसे भी मैं भैया को बाबी के विषय में स्पष्ट बता नहीं सकती थी। मैं जानती थी, मेरा परिवार कितना भी नए विचारों का हो, पर वे बाबी के साथ मेरा सम्बन्ध पसन्द नहीं करेंगे। आखिर तो वह विदेशी था और वह भी ईसाई।
इधर भैया को भी ‘ज्योति’ मिल गई थी। ‘ज्योति’ भाभी है मेरी। भैया को भी मेरी कोई विशेष आवश्यकता नहीं रही थी। हम मैत्री के स्तर से नीचे उतरकर फिर भाई-बहन होकर रह गए थे।
पर ये लोग—अश्विनी और करुणा—मित्र थे। अश्विनी को कोई ज्योति नहीं मिली थी और करुणा के पास भी उसका बाबी नहीं था। पर मैं जानती थी कि समय आएगा जब करुणा किसी की हो जाएगी और अश्विनी भी किसी और के लिए जीना चाहेगा।
अभी ऐसी कोई बात नहीं थी। वे रोज़ मिलते थे। अश्विनी जीवन के समीप आता जा रहा था। मैं रोज़ उसे देखती थी—उसे दवाई पिलाते हुए, पट्टी बदलते हुए, बिस्तर ठीक करते हुए, उसे वाश करते हुए। वह बातें नहीं करता था, बोलता नहीं था। बस देखता था। शायद वह भी समझता था कि एक पेशेवर नर्स के समान मरीज़ को देखना और उससे अधिक—सहानुभूतिपूर्वक एक व्यक्ति को जीवन के लिए प्रोत्साहित करने में फर्क था।
बात ठीक भी थी। मुझे अश्विनी ने प्रभावित किया था। जो व्यक्ति मौत से लड़ सकता है, उसे जीने के लिए सहायता क्यों न दी जाए। और अभी तो अश्विनी के दिन थे, वह शायद किसी के लिए जीना चाहे—करुणा के लिए, मां के लिए, अपने भाइयों-भाभियों के लिए और शायद किसी और के लिए भी...
और जब अश्विनी ठीक होकर घर जाने लगा तो धन्यवाद देने के लिए मेरे पास आया था वह। मुझे लगा, हम दोनों जीवन और मृत्यु के लिए एक ही रूप में सोच रहे थे। उसने कुछ ऐसा ही कहा था।
‘‘मिस वर्मा !’’ उसने मुझे सम्बोधित किया।
मैं बताना चाहती थी उसे, कि अस्पताल में किसी नर्स को बुलाने का यह गलत ढंग है। हमें डॉक्टर तक, सिस्टर अथवा सिस्टर वर्मा इत्यादि कहकर बुलाया करते हैं। जो मरीज़ अपनी किसी ग्रंथिवश सिस्टर कहकर नहीं बुलाना चाहते, वे नर्स कहकर ही पुकारते हैं।
पर मेरे कुछ कहने से पहले ही वह बोला, ‘‘यह औपचारिक धन्यवाद नहीं है, मिस वर्मा ! आपने वाकई मुझे जीवन दिया है। मैंने मरना तो कभी नहीं चाहा, किन्तु जीना तुमने ही सिखाया है मुझे।’’ वह रुका, पर जल्दी से बोला, ‘‘सच मानना, मिस वर्मा ! पहली बार तुम्हें देखकर जीने की इच्छा जागी थी मुझ में। अच्छा, मैं फिर मिलूंगा।’’ और इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, वह कमरे से निकल गया था।
मुझे बेढंगा लगा यह लड़का—हर बात में बेढंगा, क्लम्ज़ी ! चारपाई पर पड़ा था तो पड़ा ही था। मुख से कोई बात नहीं फूटती थी। अब ठीक हुआ तो आ धमका, ‘मिस वर्मा !’ मिस वर्मा का कुछ लगता है। ‘आप’ भी नहीं, ‘तुम’ । उंह ! बड़ा आया फिर मिलने वाला ! और मुझे देखकर जीने की इच्छा जागी इसमें। इन मरीजों को पता नहीं क्या बीमारी है, बस इनकी देख-भाल क्या की, समझ बैठे—अभी तक इन्हीं की प्रतीक्षा में बैठी थीं हम। रोमांटिक फूल्स ! और यह कौन-सा ढंग था ऐसी बात कहने का। आए, गोली दागी और चल दिए। वाकई इस लड़के को सेना में होना चाहिए था।
दूसरे ही दिन अश्विनी मुझसे मिलने के लिए आ पहुंचा। रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे जब फोन पर कहा कि कोई मिलने आया है तो मेरे मस्तिष्क के किसी भी कोने में अश्विनी का विचार न था।
‘‘अरे, अश्विनी, तुम !’’ जाने कहां से मेरे स्वर में आत्मीयता आ गई।
‘‘क्यों ?’’ अश्विनी आज एकदम बदला-बदला-सा था। न घायल, न मुर्झाया हुआ। पैंट-कमीज़ और टाई में सजा-संवरा अच्छा लग रहा था।
‘‘मैंने कल कहा था, शील !’’ अश्विनी ने पहली बार मुझे नाम से सम्बोधित किया, ‘‘कि मैं मिलने आऊंगा। बात यह है’’, वह रुककर बोला, ‘‘कि मैं बहुत कुछ कहना चाहता था तुम से। कल ही कहता पर मेरे घरवाले जल्दी में थे और फिर मुझे भी सोचने के लिए कुछ समय चाहिए था।’’
अश्विनी बोलता गया, मैं सुनती रही। उसकी बातों में, उसके स्वर में, कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी, जो मुझे बेढंगी लगती। कहीं गोली दागनेवाली बात नहीं आई। मुझे सबकुछ स्वाभाविक लगा। बस एक ही बात थी मन में कि यह सब तो होना ही था। शायद मैं इसी की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं इंग्लैंड और बाबी को छोड़कर इसीलिए तो अपने देश में आई थी कि मुझे कोई मिलेगा, जो भारतीय होगा। जो मुझे वैसा घर दे सकेगा, जिसकी मैं कल्पना करती हूं और जिसके साथ देखकर मेरा परिवार—मेरे माता-पिता, मेरे भाई-बहन प्रसन्न होंगे। अश्विनी वही था। वह सुन्दर है। हिम्मतवाला है। पायलट अफसर है। ठीक होकर नौकरी पर जाएगा तो पैसेवाला भी हो जाएगा। फिर सबसे बड़ी चीज़...वह भारतीय है। भारतीय रीति-रिवाजों में पला हुआ। मैं अश्विनी की ही प्रतीक्षा कर रही थी। तभी तो मैं इतना ध्यान दे सकी थी उसको....
अश्विनी ने मुझे बहुत-कुछ बताया। अपने एक्सिडेंट का विस्तार से वर्णन किया। होश में आने पर, मुझे देखने की बात बताई और फिर उसने काम करते हुए मेरी अंगुलियों को देखा था, मेरी बाहों को निहारा था; मेरे कंधे, मेरी गर्दन और मेरे मुख को देखा था। वह भी किसी के लिए जीना चाहता था। वह शायद ‘मैं’ थी। उसने बहुत पहले ही मुझसे सारी बातें कहनी चाही थीं। पूछना चाहा था कि क्या मैं उसे स्वीकार कर सकूँगी ? पर वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे कहे। सबसे बड़ा भय मेरी अस्वीकृति का था। यही कारण था कि अंत में उस बेढंगेपन से कहकर चला गया था। आज जब वह आया था और मैं उससे इस ढंग से मिली थी, तो उसने समझ लिया था कि मेरे मन में क्या था।
मैं क्या कहती ? मन डरता था। वचन कैसे दे सकती थी अश्विनी को ! अभी मैं उसके विषय में अधिक जानती भी नहीं थी। उसके माता-पिता से बात करने का कोई अवसर नहीं आया था। अभी मेरी मम्मी ने मेरे पापा ने अश्वीनी को देखा तक नहीं था। पर मैं अश्विनी को अस्वीकार भी कैसे करती। तर्क तो काम नहीं करता। भावनाओं का, इंस्टिक्ट्स का सहारा लेना पड़ेगा। और यही कारण था कि मैं अश्विनी से कुछ न कह सकी—न ‘हां’ न ‘ना’।
अंत में अश्विनी मुझसे दूसरे दिन ‘गेलार्ड’ में मिलने की बात कहकर चला गया।
मैं उसे छोड़ने के लिए बाहर तक आई। उसने जाते हुए कैसी तो आंखों से मुझे देखा और मैं घबराकर लजाती, शरमाती, मुसकाती-सी वापिस लौट आई।
बहुत देर तक बैठी सोचती रही कि अश्विनी को मिलने का वचन देकर अच्छा किया या बुरा। पर कुछ निश्चय नहीं कर पा रही थी। चाहती थी, कोई हो मेरे पास, जिसे सब कुछ बता दूं। कोई सलाह दे मुझे। कोई कह दे कि मैंने बुरा नहीं किया। कोई कहे कि अश्विनी बुरा नहीं है, अच्छा लड़का है। और कितनी कमजोर हूं मैं। बाबी से मिली थी, तब भी ऐसे ही दुर्बलता ने घेर लिया था मुझे। मैं कोई निश्चय नहीं कर पाती थी।
दूसरे दिन जब हम गेलार्ड में मिले तो अश्विनी के साथ करुणा भी थी। करुणा को देख मैं पहले भी चुकी थी, किन्तु परिचय अश्विनी ने आज ही कराया। अच्छी लग रही थी करुणा। लाल रंग की साड़ी में उसका गोरा रंग बहुत निखर आया था। यंग एंड फ्रेश, हैल्दी लुकिंग लड़की। अच्छी लगी मुझे करुणा।
अश्विनी कल से भी अच्छा लग रहा था। गोरा चिट्टा, क्लीन शेव्ड ! नेवी ब्लू सूट और नीली ही टाई, आंखों को खींचती थी।
‘‘तुम तैयार होकर नहीं आईं।’’ अश्विनी ने मुझसे कहा।
‘‘तैयार ! क्यों ?’’ मैंने स्वयं पर दृष्टि डाली। तैयार तो होकर आई थी मैं। सफ़ेद साड़ी-ब्लाउज। नई जयपुरी चप्पलें। जूड़ा भी मैंने बड़े जतन से किया था। ‘‘तैयार नहीं हूं क्या ?’’ मैंने पूछा।
‘‘कहां !’’ अश्विनी बोला, ‘‘पाउडर तक तो लगाया नहीं है तुमने। करुणा को देखो, कितनी गुडी-गुडी लग रही है।’
मैंने भरपूर दृष्टि से करुणा को देखा। करुणा अभी छोटी थी—उर्जा से भरपूर। अट्ठारह वर्षों की अल्हड़ ! मैं अट्ठाइस की थी। थक गई थी—ढीलना चाहती थी अपने आपको। मुझ में इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं बची कि सदा सजी-सजाई, तनी-तनाई रहूं। पर यदि अश्विनी इसी प्रकार प्रेमी दृष्टि के बदले आलोचक दृष्टि से मुझे देखता रहा, इसी प्रकार प्रत्येक नवयौवना से मेरी तुलना करता रहा तो हो चुका !
‘‘करुणा तो बड़ी गुड़ी गुड़ी है।’’ मैंने मुसकराने की चेष्टा की, ‘‘किन्तु मुझे गुड़ी-गुडी बनने की क्या आवश्यकता है।’’
‘‘हां, ठीक है।’’ वह शायद मेरा संकेत समझ गया था।
हम मेज़ पर बैठ गए। किन्तु मुझे अच्छा नहीं लगा। जब कभी मैं इस तरह के होटलों-रेस्तराओं में आती हूं तो मुझे लगता है कि मैं जिस वातावरण से भागकर भारत आई थी, उसने मेरा पीछा अभी तक नहीं छोड़ा है। कितना अच्छा होता यदि मुझे अश्विनी ने अपने घर बुलाया होता। मैं उसकी मां, उसकी भाभियों और करुणा के साथ बैठकर, घर की छोटी-छोटी बातों की चर्चा करती। गेलार्ड में बैठकर मेकअप में छिपी करुणा तथा टिप-टाप अश्विनी के विषय में क्या जान सकती थी। इसी नकली जीवन को जीते-जीते तंग आकर मैं छोड़ आई थी। मैं तो अब अपने इंस्टिक्ट्स के अनुसार छोटा-सा सादा जीवन जीना चाहती थी। पता नहीं मनुष्य अपने यथार्थ को स्वीकार करने से घबराता क्यों है।
‘‘शील ! डांस के लिए चलें।’’ अश्विनी कह रहा था। और तब मैंने ध्यान दिया कि डांस के लिए म्यूजिक शुरू हो गया। अंग्रेज़ी धुनों के रेकार्ड़ बजेंगे, अंग्रेज़ों की नकल करते हुए ये हिन्दुस्तानी बच्चों के समान गलत-सलत फॉक्स-ट्राट, चा-चा-चा, ट्विस्ट इत्यादि करेंगे और बड़े खुश होंगे।
‘‘पर अश्विनी...’’मैं कोई बहाना नहीं सोच पा रही थी, ‘‘मैं डांस के विचार से आई ही नहीं।’’ अंत में मुझे सत्य बात कहनी पड़ी।
सायरा कह रही थी कि जब वह लाया गया था तो और भी बुरी अवस्था में था। पायलट अफसर था कोई। जहाज़ से गिर पड़ा था और उसे खेतों में पड़े हुए को उठा लाए थे। और मैं सोच रही थी—सिविलियन जहाज़ों में तो यही बुरी बात है कि एक ही आदमी को जहाज़ देकर उड़ा देते हैं। उसे कुछ हो जाए तो बचानेवाला भी न हो। सैनिक जहाज़ों में शायद ऐसा न होता हो—मुझे पता भी क्या है। मैं कौन सी एयरफोर्स में काम कर चुकी हूं।
और अब, जब नाइट ड्यूटी पर आई तो मैंने उस नए मरीज़ को देखा। साथ ही, परिचय भी मिला। पट्टियों में बंधा पड़ा था वह। स्वभावतः मुझे उत्सुकता हुई। मैंने ध्यान से देखा उसे। कोई नई बात नहीं थी। रोज़ ही मरीज़ देखती हूं। नर्स हूं—पेशा ही यही है। बच्चा पैदा करने से पूर्व मां को तड़पते देखा है। पैदा होते हुए और धरती पर आने पर हाथ-पैर पटकते हुए बच्चे को देखा है। मां की वह गर्व भरी मुसकान भी देखी है। और उन्हें छोटे-बड़े बच्चों को निरीह, बिस्तर पर पड़े तड़पते भी देखा है। कितना बेचारा-सा लगता है व्यक्ति—अस्पताल के इन बिस्तरों पर पड़ा हुआ, जैसे बच्चा हो छोटा-सा। करवट बदल दूं तो बदल लेगा, नहीं तो एक ही करवट पड़े सोता-जागता रहेगा। और मृत्यु से लड़ता हुआ आदमी ! ओफ ! कैसे हाथ-पैर मारता है। अंत में शांत होकर पड़ा रहता है। रोज़ ही देखती हूं। सत्य तो यह है कि मरे-जीते आदमी में विशेष अंतर नहीं लगता मुझे। दो अवस्थाएं मात्र हैं आदमी की ये !
पर यह मरीज़-नया मरीज़—उन लोगों में से नहीं लगता मुझे। यह नहीं मरेगा—यह मैं जानती हूं। अपने इंस्टिक्ट से ही बता सकती हूं कि यह नहीं मरेगा, क्योंकि यह जीना चाहता है। उसके बेहोश मुख की लकीरों में ऐसी कोई बात नहीं थी, जो उसे मृत्यु से आशंकित बताती। वह जिएगा।
वैसे इस समय तो उसकी हालत खराब ही थी। पट्टियों से यूं बंधा पड़ा था कि उसकी अपनी मां भी शायद उसे इस हालत में पहचान न सके।
सोचती हूं, उसकी मां अपने घर में बैठी होगी संतोष से। क्या कर रही होगी ? शायद अपने इसी बेटे के लिए जुराबें बुन रही हो—सर्दियां आ रही हैं न ! सोचती होगी कि बेटा अपनी फ्लाइट से वापस आएगा तो उसे जुराबें देगी। और बेटा यहां पड़ा है—बेहोश ! डॉक्टर अभी तक यह आश्वासन भी नहीं दे सके कि वह जी ही पड़ेगा। पर मैं कहती हूं, वह जिएगा। नर्स किसी डॉक्टर से कम तो नहीं होती है।
पर कौन जाने उसकी मां भी किसी अनदेखे भय, किसी आशंका के कारण बिस्तर पर करवटें बदल रही हो। अपने बेटे की खैर मना रही हो। कहते हैं कि खून के रिश्ते में इस प्रकार की घटनाओं का आभास हो जाया करता है। और इसकी मां तो जानती ही होगी कि उसका बेटा हवा में उड़ रहा है—जहां किसी क्षण भी दुर्घटना हो सकती है।
पर मैं मां के विषय में ही क्यों सोच रही हूं ? मैं उसकी पत्नी के विषय में क्यों नहीं सोचती ? वह क्या कर रही होगी ? यदि विवाहित न भी हो उसकी प्रेमिका तो होगी ही। पायलट है—कोई एयर-होस्टेस या कोई और। प्रेमिका तो होगी ही—पर प्रेमिका ! पत्नी ही हो तो ठीक है।
सायरा ठीक कहती है कि मेरे इंग्लैंड जाने का कोई लाभ नहीं हुआ। छह वर्ष रहकर आई हूं इंग्लैंड में, पर अब भी दक़ियानूसी हिन्दू लड़कियों के समान मां या पत्नी की ही बात अधिक सोचती हूं, प्रेमिका की कम। मुझसे तो वे एंग्लो-इंडियन लड़कियां ही अधिक एडवांस्ड हैं, जो कभी भारत की सीमाओं को पार कर कहीं नहीं गईं—किन्तु प्रत्येक बात इंग्लैंड की दृष्टि से ही सोचती हैं।
पर सायरा एक बात नहीं जानती। मैं मां और पत्नी के रूप में अब भी नहीं सोचती—अब ही सोचती हूं। जब मैं इंग्लैंड में थी और मेरा बाबी मेरे पास था, तब तो कभी मैंने दक़ियानूसी हिन्दू लड़कियों के समान नहीं सोचा था। तब मैं अपने परिवार के बारे में, अपने भाई-बहनों के बारे में कभी नहीं सोचा था। तब मैंने बाबी के घरवालों के विषय में भी नहीं सोचा था। तब मैं थी और मेरा बाबी था। हम व्यक्ति थे, परिवारों से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं था। मैं तब प्रेमिका मात्र थी...न पत्नी थी, न कुलवधू, और इसलिए मां भी नहीं थी।
पर उन दिनों मैं जवान थी। आठ वर्ष बीत चुके हैं उस बात को। कुल बीस वर्षों की हुआ करती थी मैं। तब की बातें अब नहीं हैं। उसके पश्चात् कितना जीवन देखा है मैंने। कितना घूमी हूं। यह आठ वर्षों का, खानाबदोश का-सा जीवन। कुछ महीने कहीं, कुछ महीने कहीं। कोई घर नहीं, परिवार नहीं। जीवन से पृथक, कटे-छंटे से होटल ! वह भी कोई जीवन है—आडम्बर !
अब मैं थक गई हूं। उन दिनों के समान हर समय टिप-टाप, सजी-धजी नहीं रह सकती। हमेशा अकड़कर बैठ नहीं सकती। अट्ठाईस वर्षों का होकर, अब जीवन स्वयं को ढीलना चाहता है। रेस्तराओं, होटलों और पार्टियों के जीवन से तंग आ गई हूं। अब तो एक छोटे से घर की इच्छा होती है, जिसमें दो-एक कमरे हों—जो मेरे अपने हों, जिनकी सफाई मैं स्वयं करूं। रसोई हो, मेरी अपनी। बहुत सारे डिब्बे हों साफ़-सुथरे ! उन पर लिख-लिखकर मैं अपने हाथों से लेबिल लगाऊं। उनमें से चीज़ें निकाल-निकालकर पकाऊं और अपने पति और छोटे-छोटे दो-एक बच्चों को खिलाऊं। जब डिब्बे खाली हो जाएं तो एक-एक डिब्बा देखकर पति को लिखाऊं—दाल चने की दो सेर, दाल मसूर की डेढ़ सेर—अब स्वयं साथ जाकर सामान लाने की इच्छा नहीं होती। वे जाएं और ले आएं। रसोई तक ही सीमित हो जाऊं। इन्हीं दीवारों में घुट जाऊं।
और उस घर में एक गुसलखाना भी हो। जब वे काम पर चले जाएं तो मैं अपने गंदे बिखरे बालों का—जिनमें झाड़ू करते हुए या चूल्हा फूंकते हुए धूल और राख पड़ गई हो—रद्दी-सा जूड़ा बनाऊं और छोटे-बड़े अनेक कपड़े लेकर धोने बैठ जाऊं। उसमें उनकी बनियानें हों, कच्छे हों, रुमालें हों, पाजामें हों, कुर्ते हों। पैंट-कमीज़ तो धोबी से ही धुलवाऊंगी। चादरें हों, छोटी-छोटी कमीज़ें हों और एक छोटी-सी फ़्राक ! अंत में एक साड़ी या सलवार कमीज़ मेरी भी हो।
गार्डन हो, जिसमें....
‘‘सिस्टर ! सिस्टर !’’ वह कोने के बेडवाला मरीज़ हमेशा ही रात को पुकारता है। नींद नहीं आती बेचारे को। वह कहता है कि मैं उसे नींदवाली गोलियां दूं---किन्तु क्या लाभ है उन गोलियों का ! सिस्टम बिगड़ जाता है।
‘‘क्या बात है, बेड नम्बर तेरह ?’’ मैं मुसकराई।
मैं हमेशा बेड नम्बर से ही पुकारती हूं मरीज़ों को। अच्छा लगता है मुझको। वे भी मुसकराते हैं कि वे आदमी न होकर बेड नम्बर हो गए हैं।
‘‘नींद नहीं आती, सिस्टर !’’ बेड नम्बर तेरह मुसकराया।
आगे वह कुछ बोला नहीं, पर मैं जानती थी कि वह नींद की गोलियां मांग रहा है।
मुझे दया-सी आ गई। देखो, बेचारे को नींद के लिए भी रोज़ गोलियां मांगनी पड़ती हैं। ‘‘सो जाओ, बेड नम्बर तेरह !’’ मैंने उसके माथे पर हाथ रखा, ‘‘सोने की कोशिश करो, नींद आएगी।’’
मैंने उसका कंधा थपथपाया और लौट आई। मैं जानती थी, वह सो जाएगा।
मुझे लगता था, ये सब मेरे बच्चे हैं। मैं मां हूं इनकी। इनकी नींद सोती हूं और इन्हीं की नींद जागती हूं। ये बच्चे हैं, जिद्दी बच्चे ! सोने से पहले चाकलेट मांगते हैं, टाफियां मांगते हैं और मेरे मनाने पर मानकर सो जाते हैं।
मेरा अपना घर होगा, तो मैं अपने बच्चों को भी सुलाया करूंगी। कोई ज़िद करेगा तो उसे एक-आध चांटा लगा दूंगी। वह रो पड़ेगा तो मैं भी उसके साथ रो पड़ूंगी, ‘हाय, मेरे लाल !’
क्या हो गया है मुझे। मुझे अपने बच्चों के बदले इन मरीज़ों का ख़याल करना चाहिए। नया मरीज़ कितने मज़े से सो रहा है—हैल्दी स्लीप ! उसे कोई खतरा नहीं है। वह जिएगा, क्योंकि वह शायद किसी के लिए जीना चाहता है। मैं भी किसी के लिए जीना चाहती हूं। कितने समीप हैं हम !
दूसरे दिन जब मैं आई तो मेरा ध्यान सबसे पहले नए मरीज़ की ओर गया। वह खतरे की सीमाओं को बहुत पीछे छोड़ आया था। मैं सोचती हूं कि यदि सिविलियन के स्थान पर वह सैनिक पायलट होता तो ज़्यादा अच्छा होता। वह मृत्यु से किस प्रकार जूझा था, यह मैंने देखा था। एक क्षण के लिए भी वह निराश नहीं हुआ था। ठीक कहा था डॉक्टर पुरी ने, ‘ही हैज़ विल !’ और अब तो कोई बात ही नहीं थी। घाव अब भी उतने ही गहरे थे। पीड़ा अब भी उसे उतनी ही हो रही होगी, किन्तु जान का खतरा अब नहीं रह गया था उसे।
धीरे-धीरे नया मरीज़ भी पुराना हो गया था। उसके परिवार वालों का पता लग गया था। वे आते थे उससे मिलने। मां थी उसकी—बूढ़ी-सी। एक बहन थी छोटी। सुन्दर नहीं कही जा सकती, किन्तु आकर्षक अवश्य थी। गोरी झक्क ! अच्छी फैशनेबुल लड़की थी। और उसके दो भाई आए थे मिलने।
अश्विनी...नया मरीज...अधिक बातें नहीं करता था। बस मुसकराता जाता था। मैंने उसे अपनी मां से भी अधिक बातें करते नहीं देखा था। भाइयों के दुर्घटना के विषय में पूछने पर बस यही कहा था उसने, ‘मशीनरी गड़बड़ा गई और गिर गए।’ और अंत में एक मुसकान जोड़ दी थी उसने।
बहन बहुत सारी बातें करती रही थी। वह सुनता रहा था। मुझे लगा, उसकी यह छोटी बहन ही सबसे अधिक समीप है उसके। वे शायद भाई-बहन के औपचारिक रिश्ते से ऊपर उठकर मैत्री स्तर पर आ चुके थे। अच्छा लगा मुझे। इंग्लैंड जाने से पहले, मेरी भी भैया से ऐसी ही दोस्ती थी। पर फिर मैं इंग्लैंड चली गई थी। मुझे बाबी मिल गया था। मुझे और किसी की ज़रूरत भी नहीं रही थी और वैसे भी मैं भैया को बाबी के विषय में स्पष्ट बता नहीं सकती थी। मैं जानती थी, मेरा परिवार कितना भी नए विचारों का हो, पर वे बाबी के साथ मेरा सम्बन्ध पसन्द नहीं करेंगे। आखिर तो वह विदेशी था और वह भी ईसाई।
इधर भैया को भी ‘ज्योति’ मिल गई थी। ‘ज्योति’ भाभी है मेरी। भैया को भी मेरी कोई विशेष आवश्यकता नहीं रही थी। हम मैत्री के स्तर से नीचे उतरकर फिर भाई-बहन होकर रह गए थे।
पर ये लोग—अश्विनी और करुणा—मित्र थे। अश्विनी को कोई ज्योति नहीं मिली थी और करुणा के पास भी उसका बाबी नहीं था। पर मैं जानती थी कि समय आएगा जब करुणा किसी की हो जाएगी और अश्विनी भी किसी और के लिए जीना चाहेगा।
अभी ऐसी कोई बात नहीं थी। वे रोज़ मिलते थे। अश्विनी जीवन के समीप आता जा रहा था। मैं रोज़ उसे देखती थी—उसे दवाई पिलाते हुए, पट्टी बदलते हुए, बिस्तर ठीक करते हुए, उसे वाश करते हुए। वह बातें नहीं करता था, बोलता नहीं था। बस देखता था। शायद वह भी समझता था कि एक पेशेवर नर्स के समान मरीज़ को देखना और उससे अधिक—सहानुभूतिपूर्वक एक व्यक्ति को जीवन के लिए प्रोत्साहित करने में फर्क था।
बात ठीक भी थी। मुझे अश्विनी ने प्रभावित किया था। जो व्यक्ति मौत से लड़ सकता है, उसे जीने के लिए सहायता क्यों न दी जाए। और अभी तो अश्विनी के दिन थे, वह शायद किसी के लिए जीना चाहे—करुणा के लिए, मां के लिए, अपने भाइयों-भाभियों के लिए और शायद किसी और के लिए भी...
और जब अश्विनी ठीक होकर घर जाने लगा तो धन्यवाद देने के लिए मेरे पास आया था वह। मुझे लगा, हम दोनों जीवन और मृत्यु के लिए एक ही रूप में सोच रहे थे। उसने कुछ ऐसा ही कहा था।
‘‘मिस वर्मा !’’ उसने मुझे सम्बोधित किया।
मैं बताना चाहती थी उसे, कि अस्पताल में किसी नर्स को बुलाने का यह गलत ढंग है। हमें डॉक्टर तक, सिस्टर अथवा सिस्टर वर्मा इत्यादि कहकर बुलाया करते हैं। जो मरीज़ अपनी किसी ग्रंथिवश सिस्टर कहकर नहीं बुलाना चाहते, वे नर्स कहकर ही पुकारते हैं।
पर मेरे कुछ कहने से पहले ही वह बोला, ‘‘यह औपचारिक धन्यवाद नहीं है, मिस वर्मा ! आपने वाकई मुझे जीवन दिया है। मैंने मरना तो कभी नहीं चाहा, किन्तु जीना तुमने ही सिखाया है मुझे।’’ वह रुका, पर जल्दी से बोला, ‘‘सच मानना, मिस वर्मा ! पहली बार तुम्हें देखकर जीने की इच्छा जागी थी मुझ में। अच्छा, मैं फिर मिलूंगा।’’ और इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, वह कमरे से निकल गया था।
मुझे बेढंगा लगा यह लड़का—हर बात में बेढंगा, क्लम्ज़ी ! चारपाई पर पड़ा था तो पड़ा ही था। मुख से कोई बात नहीं फूटती थी। अब ठीक हुआ तो आ धमका, ‘मिस वर्मा !’ मिस वर्मा का कुछ लगता है। ‘आप’ भी नहीं, ‘तुम’ । उंह ! बड़ा आया फिर मिलने वाला ! और मुझे देखकर जीने की इच्छा जागी इसमें। इन मरीजों को पता नहीं क्या बीमारी है, बस इनकी देख-भाल क्या की, समझ बैठे—अभी तक इन्हीं की प्रतीक्षा में बैठी थीं हम। रोमांटिक फूल्स ! और यह कौन-सा ढंग था ऐसी बात कहने का। आए, गोली दागी और चल दिए। वाकई इस लड़के को सेना में होना चाहिए था।
दूसरे ही दिन अश्विनी मुझसे मिलने के लिए आ पहुंचा। रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे जब फोन पर कहा कि कोई मिलने आया है तो मेरे मस्तिष्क के किसी भी कोने में अश्विनी का विचार न था।
‘‘अरे, अश्विनी, तुम !’’ जाने कहां से मेरे स्वर में आत्मीयता आ गई।
‘‘क्यों ?’’ अश्विनी आज एकदम बदला-बदला-सा था। न घायल, न मुर्झाया हुआ। पैंट-कमीज़ और टाई में सजा-संवरा अच्छा लग रहा था।
‘‘मैंने कल कहा था, शील !’’ अश्विनी ने पहली बार मुझे नाम से सम्बोधित किया, ‘‘कि मैं मिलने आऊंगा। बात यह है’’, वह रुककर बोला, ‘‘कि मैं बहुत कुछ कहना चाहता था तुम से। कल ही कहता पर मेरे घरवाले जल्दी में थे और फिर मुझे भी सोचने के लिए कुछ समय चाहिए था।’’
अश्विनी बोलता गया, मैं सुनती रही। उसकी बातों में, उसके स्वर में, कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी, जो मुझे बेढंगी लगती। कहीं गोली दागनेवाली बात नहीं आई। मुझे सबकुछ स्वाभाविक लगा। बस एक ही बात थी मन में कि यह सब तो होना ही था। शायद मैं इसी की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं इंग्लैंड और बाबी को छोड़कर इसीलिए तो अपने देश में आई थी कि मुझे कोई मिलेगा, जो भारतीय होगा। जो मुझे वैसा घर दे सकेगा, जिसकी मैं कल्पना करती हूं और जिसके साथ देखकर मेरा परिवार—मेरे माता-पिता, मेरे भाई-बहन प्रसन्न होंगे। अश्विनी वही था। वह सुन्दर है। हिम्मतवाला है। पायलट अफसर है। ठीक होकर नौकरी पर जाएगा तो पैसेवाला भी हो जाएगा। फिर सबसे बड़ी चीज़...वह भारतीय है। भारतीय रीति-रिवाजों में पला हुआ। मैं अश्विनी की ही प्रतीक्षा कर रही थी। तभी तो मैं इतना ध्यान दे सकी थी उसको....
अश्विनी ने मुझे बहुत-कुछ बताया। अपने एक्सिडेंट का विस्तार से वर्णन किया। होश में आने पर, मुझे देखने की बात बताई और फिर उसने काम करते हुए मेरी अंगुलियों को देखा था, मेरी बाहों को निहारा था; मेरे कंधे, मेरी गर्दन और मेरे मुख को देखा था। वह भी किसी के लिए जीना चाहता था। वह शायद ‘मैं’ थी। उसने बहुत पहले ही मुझसे सारी बातें कहनी चाही थीं। पूछना चाहा था कि क्या मैं उसे स्वीकार कर सकूँगी ? पर वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे कहे। सबसे बड़ा भय मेरी अस्वीकृति का था। यही कारण था कि अंत में उस बेढंगेपन से कहकर चला गया था। आज जब वह आया था और मैं उससे इस ढंग से मिली थी, तो उसने समझ लिया था कि मेरे मन में क्या था।
मैं क्या कहती ? मन डरता था। वचन कैसे दे सकती थी अश्विनी को ! अभी मैं उसके विषय में अधिक जानती भी नहीं थी। उसके माता-पिता से बात करने का कोई अवसर नहीं आया था। अभी मेरी मम्मी ने मेरे पापा ने अश्वीनी को देखा तक नहीं था। पर मैं अश्विनी को अस्वीकार भी कैसे करती। तर्क तो काम नहीं करता। भावनाओं का, इंस्टिक्ट्स का सहारा लेना पड़ेगा। और यही कारण था कि मैं अश्विनी से कुछ न कह सकी—न ‘हां’ न ‘ना’।
अंत में अश्विनी मुझसे दूसरे दिन ‘गेलार्ड’ में मिलने की बात कहकर चला गया।
मैं उसे छोड़ने के लिए बाहर तक आई। उसने जाते हुए कैसी तो आंखों से मुझे देखा और मैं घबराकर लजाती, शरमाती, मुसकाती-सी वापिस लौट आई।
बहुत देर तक बैठी सोचती रही कि अश्विनी को मिलने का वचन देकर अच्छा किया या बुरा। पर कुछ निश्चय नहीं कर पा रही थी। चाहती थी, कोई हो मेरे पास, जिसे सब कुछ बता दूं। कोई सलाह दे मुझे। कोई कह दे कि मैंने बुरा नहीं किया। कोई कहे कि अश्विनी बुरा नहीं है, अच्छा लड़का है। और कितनी कमजोर हूं मैं। बाबी से मिली थी, तब भी ऐसे ही दुर्बलता ने घेर लिया था मुझे। मैं कोई निश्चय नहीं कर पाती थी।
दूसरे दिन जब हम गेलार्ड में मिले तो अश्विनी के साथ करुणा भी थी। करुणा को देख मैं पहले भी चुकी थी, किन्तु परिचय अश्विनी ने आज ही कराया। अच्छी लग रही थी करुणा। लाल रंग की साड़ी में उसका गोरा रंग बहुत निखर आया था। यंग एंड फ्रेश, हैल्दी लुकिंग लड़की। अच्छी लगी मुझे करुणा।
अश्विनी कल से भी अच्छा लग रहा था। गोरा चिट्टा, क्लीन शेव्ड ! नेवी ब्लू सूट और नीली ही टाई, आंखों को खींचती थी।
‘‘तुम तैयार होकर नहीं आईं।’’ अश्विनी ने मुझसे कहा।
‘‘तैयार ! क्यों ?’’ मैंने स्वयं पर दृष्टि डाली। तैयार तो होकर आई थी मैं। सफ़ेद साड़ी-ब्लाउज। नई जयपुरी चप्पलें। जूड़ा भी मैंने बड़े जतन से किया था। ‘‘तैयार नहीं हूं क्या ?’’ मैंने पूछा।
‘‘कहां !’’ अश्विनी बोला, ‘‘पाउडर तक तो लगाया नहीं है तुमने। करुणा को देखो, कितनी गुडी-गुडी लग रही है।’
मैंने भरपूर दृष्टि से करुणा को देखा। करुणा अभी छोटी थी—उर्जा से भरपूर। अट्ठारह वर्षों की अल्हड़ ! मैं अट्ठाइस की थी। थक गई थी—ढीलना चाहती थी अपने आपको। मुझ में इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं बची कि सदा सजी-सजाई, तनी-तनाई रहूं। पर यदि अश्विनी इसी प्रकार प्रेमी दृष्टि के बदले आलोचक दृष्टि से मुझे देखता रहा, इसी प्रकार प्रत्येक नवयौवना से मेरी तुलना करता रहा तो हो चुका !
‘‘करुणा तो बड़ी गुड़ी गुड़ी है।’’ मैंने मुसकराने की चेष्टा की, ‘‘किन्तु मुझे गुड़ी-गुडी बनने की क्या आवश्यकता है।’’
‘‘हां, ठीक है।’’ वह शायद मेरा संकेत समझ गया था।
हम मेज़ पर बैठ गए। किन्तु मुझे अच्छा नहीं लगा। जब कभी मैं इस तरह के होटलों-रेस्तराओं में आती हूं तो मुझे लगता है कि मैं जिस वातावरण से भागकर भारत आई थी, उसने मेरा पीछा अभी तक नहीं छोड़ा है। कितना अच्छा होता यदि मुझे अश्विनी ने अपने घर बुलाया होता। मैं उसकी मां, उसकी भाभियों और करुणा के साथ बैठकर, घर की छोटी-छोटी बातों की चर्चा करती। गेलार्ड में बैठकर मेकअप में छिपी करुणा तथा टिप-टाप अश्विनी के विषय में क्या जान सकती थी। इसी नकली जीवन को जीते-जीते तंग आकर मैं छोड़ आई थी। मैं तो अब अपने इंस्टिक्ट्स के अनुसार छोटा-सा सादा जीवन जीना चाहती थी। पता नहीं मनुष्य अपने यथार्थ को स्वीकार करने से घबराता क्यों है।
‘‘शील ! डांस के लिए चलें।’’ अश्विनी कह रहा था। और तब मैंने ध्यान दिया कि डांस के लिए म्यूजिक शुरू हो गया। अंग्रेज़ी धुनों के रेकार्ड़ बजेंगे, अंग्रेज़ों की नकल करते हुए ये हिन्दुस्तानी बच्चों के समान गलत-सलत फॉक्स-ट्राट, चा-चा-चा, ट्विस्ट इत्यादि करेंगे और बड़े खुश होंगे।
‘‘पर अश्विनी...’’मैं कोई बहाना नहीं सोच पा रही थी, ‘‘मैं डांस के विचार से आई ही नहीं।’’ अंत में मुझे सत्य बात कहनी पड़ी।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i